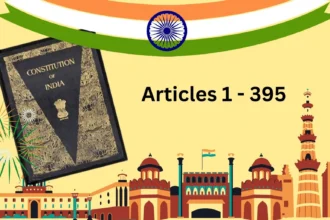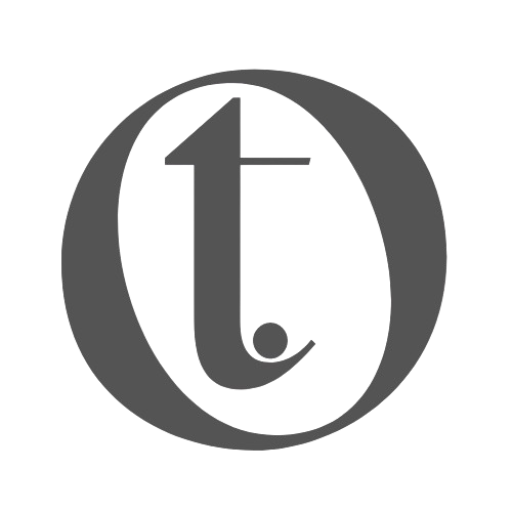अनुच्छेद 17 (Article-17 in Hindi) – अस्पृश्यता का अंत
‘अस्पृश्यता’ का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ‘अस्पृश्यता’ से उपजी किसी निर्योषयता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
अनुच्छेद 17 में “छुआछूत” पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और किसी भी तरीके से इसके अभ्यास की मनाही है। यदि छुआछूत के आधार पर कोई विकलांगता उत्पन्न होती है तो यह एक अपराध होगा जो कानून के तहत दंडनीय होगा। यह एक साधारण दावे के साथ बंद नहीं करता है अभी तक इस निषिद्ध ‘ अप्राप्यता ‘ की घोषणा के फलस्वरूप किसी भी तरीके से अभ्यास नहीं किया जा रहा है।
व्याख्या
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी प्रकार की निर्योग्यता को लागू करना न केवल अवैध है, बल्कि यह एक दंडनीय अपराध भी है।
अनुच्छेद 17 का मुख्य प्रावधान
- अस्पृश्यता का निषेध:
- अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त किया गया है।
- अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सामाजिक, धार्मिक, या अन्य प्रकार की सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता।
- अपराध और दंड:
- अस्पृश्यता का कोई भी आचरण दंडनीय अपराध होगा।
- इसके लिए विधि के अनुसार सख्त दंड का प्रावधान है।
- नागरिक अधिकारों की रक्षा:
- 1976 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन करके इसे नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, 1955 का नाम दिया गया।
- इसमें दंड संबंधी प्रावधानों को सख्त किया गया।
अस्पृश्यता की परिभाषा
संविधान और कानून में “अस्पृश्यता” की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।
- मैसूर उच्च न्यायालय की व्याख्या:
अस्पृश्यता का तात्पर्य ऐतिहासिक रूप से उन सामाजिक निर्योग्यताओं से है जो कुछ जातियों के आधार पर लोगों पर थोप दी गई थीं।- इसमें सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक सेवाओं से वंचित करना शामिल है।
उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था
- राज्य और नागरिकों का दायित्व:
- यह निजी व्यक्तियों और राज्य दोनों का दायित्व है कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
- किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोकना संवैधानिक दायित्व है।
- समाज सुधार का उद्देश्य:
- अनुच्छेद 17 सामाजिक समानता और गरिमा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, 1955 के प्रमुख प्रावधान
- अस्पृश्यता के किसी भी रूप को अपराध घोषित किया गया।
- दंडात्मक प्रावधान:
- दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान।
- सख्त दंडात्मक उपायों के जरिए सामाजिक समानता को सुनिश्चित किया गया।
- अधिनियम का प्रभाव:
- अस्पृश्यता के सभी रूपों को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया।
- समाज में पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसे लागू किया गया।
संविधान में अस्पृश्यता का अंत क्यों आवश्यक था?
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
- अस्पृश्यता भारतीय समाज में सदियों से व्याप्त थी और जाति व्यवस्था के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था।
- सामाजिक समानता का लक्ष्य:
- भारत के संविधान का उद्देश्य एक समतावादी समाज की स्थापना करना है, जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो।
- राष्ट्र निर्माण:
- अस्पृश्यता को समाप्त करना राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अनिवार्य था।
अनुच्छेद 17 न केवल अस्पृश्यता को समाप्त करता है, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रयास करता है, जहां हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान मिले। नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम, 1955 जैसे कानून इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं।
Click here to read more from the Constitution Of India & Constitution of India in Hindi
Source : – भारत का संविधान