प्राचीन भारतीय इतिहास (Indian Ancient History) की जानकारी के बारे में जानने के लिए विभिन्न स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। जिनमें से ये तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं-
- पुरातात्विक स्रोत,
- साहित्यिक स्रोत तथा
- विदेशी यात्रियों के विवरण।
पुरातात्विक स्रोत (Indian Ancient History)
प्राचीन भारत (Indian Ancient History) के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का सर्वाधिक प्रमाणिक हैं। जिनमें से मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं।
अभिलेख
- पुरातात्विक स्रोतों को जानने मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। प्राचीन भारत (Indian Ancient History के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तम्भों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण किए हैं।
- सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के “बोगजकोई नामक” स्थान से लगभग 1400 ई.पू. में मिले हैं। इस अभिलेख में इन्द्र, मित्र, वरूण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं।
- भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक (300 ई.पू.) के हैं। मास्की, गुज्जर्रा, निट्टूर एवं उदेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। इन अभिलेखों से अशोक के धर्म और राजत्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।
- अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। केवल उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की तरह दाईं से बाई की ओर लिखी जाती है।
- लघमान एवं शरेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में हैं। इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में मिले हैं।
- प्रारम्भिक अभिलेख (गुप्त काल से पूर्व) प्राकृत भाषा में हैं किन्तु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं।
- कुछ गैर सरकारी अभिलेख जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेसनगर (विदिशा) से प्राप्त गरूड़ स्तम्भ लेख जिसमें द्वितीय शताब्दी ई.पू. में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त बाराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमाण के लेखों का विवरण है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मिले हैं।
- पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिन्धु नदी के घाटी पर अधिकार कर लिया था। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी करवाया। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलखों को पढ़ा था।
सिक्के
- सिक्के के अध्ययन को “मुद्राशास्त्र” कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। पकाई गयी मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे ईसा की आरम्भिक तीन सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं।
- आरम्भिक सिक्कों पर चिन्ह मात्र मिलते हैं किन्तु बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लेखित मिलती है।
- आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के-भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं जो ई.पू. पांचवी सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाये जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें “आहत मुद्रा” कहते हैं।
- आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां (होर्ड्स) पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली हैं। आरम्भिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते हैं जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के “पंचमार्क सिक्के” कहलाते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्द्धचन्द्र आदि आकृतियां बनी होती थी।
- सर्वाधिक सिक्के मौर्यात्तर काल में मिले हैं जो विशेषतः सीसे, चांदी, तांबा एवं सोने के हैं। सातवाहनों ने सीसे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किये। सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के हिन्द-यूनानी (इण्डो-ग्रीक) शासकों ने चलाए।
स्मारक एवं भवन
- प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर ‘नागर शैली’ दक्षिण भारत के ‘द्रविड़ शैली’ तथा मध्य भारत के मंदिर ‘वेसर शैली’ में है।
- दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार की जानकारी प्राप्त होती है।
मूर्तियां
- प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण की शुरुआत कुषाण काल से होती है। कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है।
- कुषाण कालीन गान्धार कला पर विदेशी प्रभाव है जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है।
चित्रकला
- चित्रकला से हमें तत्कालीन जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अजन्ता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रकला में “माता और शिशु” तथा “मरणासन्न राजकुमारी” जैसे चित्रों से गुप्तकाल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है।
अवशेष
- अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। हड़प्पा, मोहन जोदड़ों से प्राप्त मुहरों से उनके धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। बसाढ़ से प्राप्त मिट्टी की मुहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है।
साहित्यिक स्रोत (Indian Ancient History)
साहित्यिक स्रोतों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है-
- धार्मिक साहित्य
- धर्मोतर साहित्य या लौकिक साहित्य
धार्मिक साहित्य
- धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रन्थों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रन्थ आते हैं।
- ब्राह्मणेत्तर ग्रन्थों में बौद्ध एवं जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रन्थों, जीवनियां, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है।
ब्राह्मण साहित्य
- वेद चार हैं – ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एक मात्र स्रोत वेद है।
- ब्राह्मण साहित्य (वेद) में सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है।
ऋग्वेद
- इसकी रचना 1500 ई.पू. से 1000 ई.पू. के बीच माना जाता हैं। ऋक् का अर्थ है “छन्दों एवं चरणों से युक्त मंत्र”। यह एक ऐसा ज्ञान (वेद) है जो ऋचाओं से बद्ध है इसलिए यह ऋग्वेद कहलाता है।
- ऋग्वेद में कुल दस मण्डल एवं 1028 सूक्त और कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होतृ ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था।
- ऋग्वेद में पहला, आठवाँ, नवां एवं दसवां मण्डल सबसे अन्त में जोड़ा गया है। वेद मंत्रों के समूह को ‘सूक्त’ कहा जाता है, जिसमें एकदैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है।
- प्रथम और अन्तिम मण्डल, दोनों ही समान रूप से बड़े हैं। उनमें सूक्तों की संख्या भी 191 है। दूसरे मण्डल से सातवें मण्डल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है, उसका हृदय है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रन्थ हैं – “ऐतरेय एवं कौषीतिकी अथवा शंखायन”।
यजुर्वेद
- यजु का अर्थ है “यज्ञ”। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि-विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के मन्त्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित “अध्वर्य” कहलाता है। इसके दो भाग हैं – शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद कर्मकाण्ड प्रधान है।
- यह पांच शाखाओं में विभक्त है- 1. काठक 2. कपिष्ठल 3. मैत्रायणी 4. तैत्तिरीय 5. वाजसनेयी। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठ, इशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गये हैं।
सामवेद
- साम का शाब्दिक अर्थ है “गान”। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाये जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे “भारतीय संगीत का मूल” कहा जा सकता है।
- सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छन्दोग्य तथा जैमिनीय उपनिषद हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रन्थ पंचविश है।
अथर्ववेद
- इसकी रचना सबसे अन्त में हुई। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्य एवं अनार्य विचार-धाराओं का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरूओं का राजा कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है।
- इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाजनिष्ठा,औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू-टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन है।
- अथर्ववेद का एक मात्र ब्राह्मण ग्रन्थ गोपथ है। इनके उपनिषदों में मुख्य हैं मुण्डकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्योपनिषद।
ब्राह्मण ग्रन्थ
इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है “यज्ञ”। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ “ब्राह्मण” कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग-अलग ब्राह्मण ग्रन्थ हैं।
ऐतरेय ब्राह्मण में राज्यभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिये गये हैं। शतपथ ब्राह्मण में गान्धार, शल्य, कैकेय, कुरू, पांचाल, कोशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है।
आरण्यक
- यह ब्राह्मण ग्रन्थ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिन्तनशील ज्ञान के पक्ष में अधिक महत्व दिया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है।
- आरण्यक कुल सात हैं- 1. ऐतरेय, 2. शांखायन, 3. तैत्तिरीय, 4. मैत्रायणी, 5. माध्यन्दिन वृहदारण्यक, 6. तल्वकार, 7. छन्दोग्य।
उपनिषद
- उप का अर्थ है “समीप” और निषद का अर्थ है “बैठना”। अर्थात् जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरू के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, उसे “उपनिषद” कहते हैं।
- उपनिषद आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें “वेदान्त” भी कहा जाता है।
- उपनिषद उत्तरवैदिक काल की रचनाएं हैं इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे “पराविद्या या आध्यात्म विद्या” भी कहते हैं।
- भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य “सत्यमेव जयते” मुण्डकोपनिषद से उद्धत है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष एवं पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है।
- उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है किन्तु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। प्रमुख उपनिषद हैं – ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, कौषीतकी, वृहदारण्यक, श्वेताश्वर आदि।
वेदांग
इनकी संख्या छः है – शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, ज्योतिष एवं छन्द। ये गद्य में सूत्र रूप में लिखे गये हैं।
- शिक्षा – वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ।
- कल्प – ये ऐसे कल्प (सूत्र) होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है।
- व्याकरण – इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गये हैं।
- निरूक्त – शब्दों का अर्थ क्यों होता है, यह बताने वाले शास्त्र को निरूक्त कहते हैं। यह एक प्रकार का भाषा-विज्ञान है।
- छन्द – वैदिक साहित्य में गायत्री तिष्टुप, जगती, वृहती आदि छन्दों का प्रयोग हुआ है।
- ज्योतिष – इसमें ज्योतिषशास्त्र के विकास को दिखाया गया है।
सूत्र
वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाते हैं। कल्पसूत्रों के तीन भाग हैं-
- श्रौत सूत्र – यज्ञ संबंधी नियम।
- गृहय सूत्र – लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन।
- धर्म सूत्र – धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख।
धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रन्थों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रन्थ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, वृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति आदि। व्याकरण ग्रन्थों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना 400 ई.पू. के लगभग की गयी थी। सूत्र साहित्य में आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है।
मनुस्मृति के भाष्यकार (टीकाकार) मेधातिथि, गोविन्दराज, भारूचि एवं कुल्लूक भट्ट थे। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर (मिताक्षरा) एवं अपरार्क आदि थे। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है।
प्रमुख उपवेद हैं – आयुर्वेद, धनुर्वेद,गन्धर्ववेद तथा शिल्पवेद।

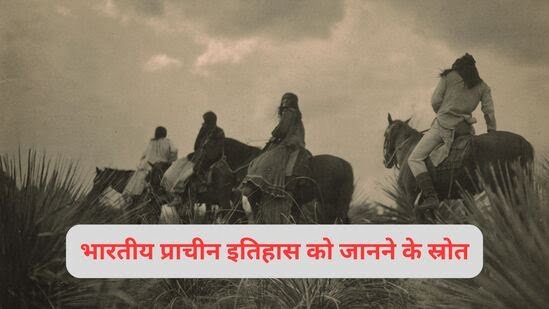


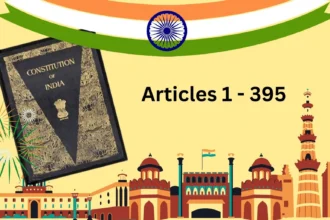
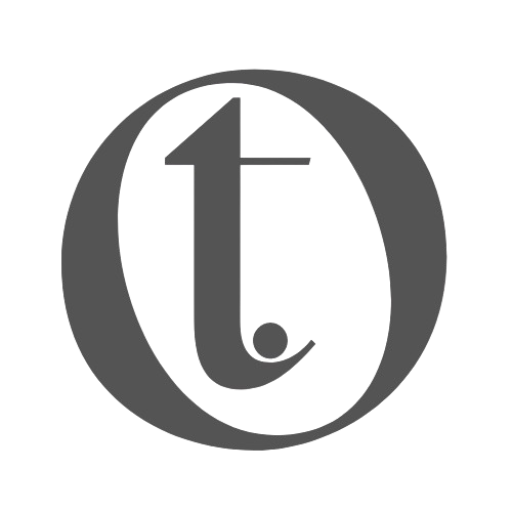
I am not sure where youre getting your info but good topic I needs to spend some time learning much more or understanding more Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission